भारत में शासन संविधान का है, सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी किए जाएंगे?
इस तरह देखें तो भारत के राष्ट्रपति की अपार शक्तियां हैं, जिन्हें किसी भी न्यायालय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह उससे भी ऊपर है।
Total Views |

जब देश की कोई व्यवस्था संविधान से ऊपर नहीं, तब क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर हो सकता है?
स्वाभाविक है, नहीं। उसका काम संविधान के प्रावधानों का अनुपालन कराना है, और उसके प्रकाश में निर्णय सुनाना है, किंतु यदि यही सुप्रीम कोर्ट निरंकुश हो जाए, अपने हिसाब से मनमाने निर्णय देने लगे और उसके पीछे तर्क संविधान का गढ़े, तब फिर क्या किया जाना चाहिए?
क्या सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने का हक किसी को है? क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका तो यह करने से रहे!
प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किंतु उतनी ही जितनी कि देश के एक आम व्यक्ति को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मामले या कहें न्यायालय के किसी भी मामले में वह बहुत सीमित है।
इतनी ही कि कोई फैसला आया तो वह सिर्फ रिपोर्टिंग करे, उसमें भी ध्यान रखे कि कहीं कुछ ऐसा न लिख दे, जिससे कि न्यायालय को लगे कि उसकी अवमानना हो रही है और वह अवमानना का हवाला देकर खबर लिखने वाले पत्रकार को ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे, तब फिर क्या किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सके?
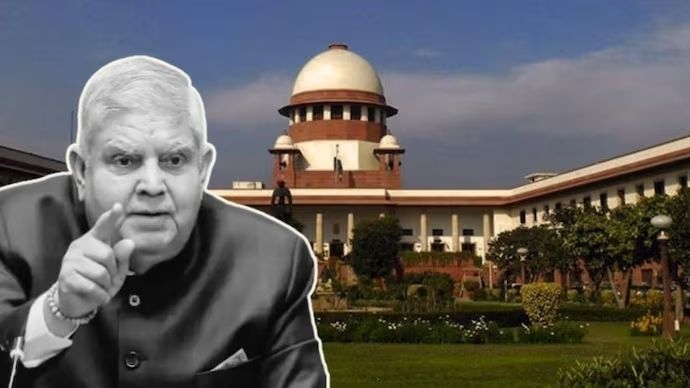
वास्तव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहकर एक नई बहस को जन्म दिया है कि ‘देश ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम भी खुद ही करेंगे और सुपर संसद की तरह काम करेंगे। अनुच्छेद-142 न्यायपालिका के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।’
यहां उपराष्ट्रपति धनखड़ जो कह रहे हैं, उसके विरोध में यह तय है कि कई लोग, संगठन, राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, जिन्हें उनकी बात नहीं पसंद आएगी।
पर फिर भी यह विचार जरूर करें कि क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ कुछ गलत बोल रहे हैं।
यह भारतीय संविधान का ही प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, राज्यपाल किसी भी राज्य का और महापौर नगरपालिका निगम में उस नगर का प्रथम नागरिक है, पर उस प्रथम नागरिक की हैसियत इन न्यायपालिकाओं ने क्या बना रखी है, वह इनके अनेक निर्णयों को देखकर एवं उसके गहन अध्ययन से आज आप सहज ही समझ सकते हैं।
जिसके बाद आपको यही लगेगा कि यह (प्रथम नागरिक होना) सिर्फ औपचारिकता भर है।

वास्तव में पहला, दूसरा या तीसरा यदि कोई नागरिक और उसकी निहित शक्ति है तो वह सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला न्यायालय एवं इसी तरह से अन्य न्यायिक व्यवस्था कानूनी तंत्र है, ये सभी किस कानून का हवाला देकर आपकी कैसे गर्दन मरोड़ेंगे, आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं!
देश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग कार्य निर्धारित हैं।
यदि नियमों की बात की जाए तो भारत में विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती है।
इन तीनों के ऊपर है भारत का राष्ट्रपति, इसलिए ही वह (राष्ट्रपति) संघ का प्रमुख है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित बताई गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
वह न्यायालय के सम्मान में ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
राष्ट्रपति के पास यह शक्ति भी है कि वह किस न्यायाधीश को उसके पद से हटाएं अथवा नहीं, यानी कि न्यायाधीशों को उनके पद से समय पूर्व या किसी भी अन्य कारण से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति अपने पास रखते हैं।
जब देश में किसी भी मामले में कानून संबंधी सवाल खड़े होते हैं तब भी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह तय करेंगे कि देश को किस ओर ले जाना है, इसके लिए राष्ट्रपति अदालत को निर्देशित भी कर सकते हैं।
इतना सब होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले में सिर्फ राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग कर अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं।

फिर राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होने की भी शक्ति है।
इस तरह देखें तो भारत के राष्ट्रपति की अपार शक्तियां हैं, जिन्हें किसी भी न्यायालय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह उससे भी ऊपर है।
भारतीय संविधान कहता है कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की सबसे बड़ी इकाई होने के नाते देश के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे अथवा नहीं, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
यानी कि न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए स्पष्ट रूप से बाध्यकारी नहीं है।
कुल मिलाकर राष्ट्रपति में संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति निहित है, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय तीनों की शक्ति राष्ट्रपति पद में निहित है।
पर यहां व्यवहार में क्या हो रहा है? जिस राष्ट्रपति को विधायिका चुनती है, और यह विधायिका किसी भी लोकतंत्र शासन प्रणाली में उस लोक के एक-एक चुने हुए जन प्रतिनिधि से बनती है, उस विधायिका की शक्ति को ही न्यायालय आज खुद से संचालित करते हुए देखा जा रहा है।

यह ठीक वैसे ही है जैसे कि एक पिता को उसका पुत्र निर्देशित करे कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, जबकि ऐसा करते वक्त पुत्र यह भूल जाता है कि यदि समाज की शक्ति पिता बनने का अवसर ही नहीं देती तो पुत्र इस संसार में आता ही नहीं।
यानी कि जिस विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि जनतंत्र को संचालित करने का काम करते हैं, आज न्यायालय उस पर ही कई तरह से अंकुश लगाने का काम कर रहा है।
वास्तव में इसी का यह सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समयसीमा तय कर दी।
वस्तुत: इसी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्हें कहना पड़ा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें।
अब भले ही अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता हो कि वह पूर्ण न्याय (कम्पलीट जस्टिस) करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो।
पर उसे भी यह सदैव याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम है और सभी संस्थाओं को अपनी-अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है।
उपराष्ट्रपति धनखड़ आज राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लिए जाने के वास्ते समयसीमा निर्धारित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चिंता जता रहे हैं, जो वाकई गंभीर है।
क्योंकि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे।
आश्चर्य है, राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है।

धनखड़ पूछ रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? देश में ये क्या हो रहा है? हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता!
वे सही कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं।
‘हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करने का है उसके आधार पर। फिर भी इसके लिए पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।’
उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जब अनुच्छेद 145(3) तय हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या आठ थी, उसमें भी इस प्रकार के निर्णय के लिए पांच या उससे भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, पर अब तो 30 से ऊपर हैं, तब फिर समझ लीजिए कि यदि इस तरह का कोई निर्णय न्यायपालिका को लेना हो तो कितने जज होने चाहिए?
पर जो फैसला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और उसमें जिस तरह से राष्ट्रपति की शक्तियों को छोटा कर दिखाने का प्रयास हुआ है, वह कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकेगा।
अब भले ही केंद्र सरकार कोई विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं पलटे, लेकिन इस पर जरूर विचार किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेपी पारदीवाला की दो सदस्यीय बेंच यह फैसला सुना कैसे सकती है?
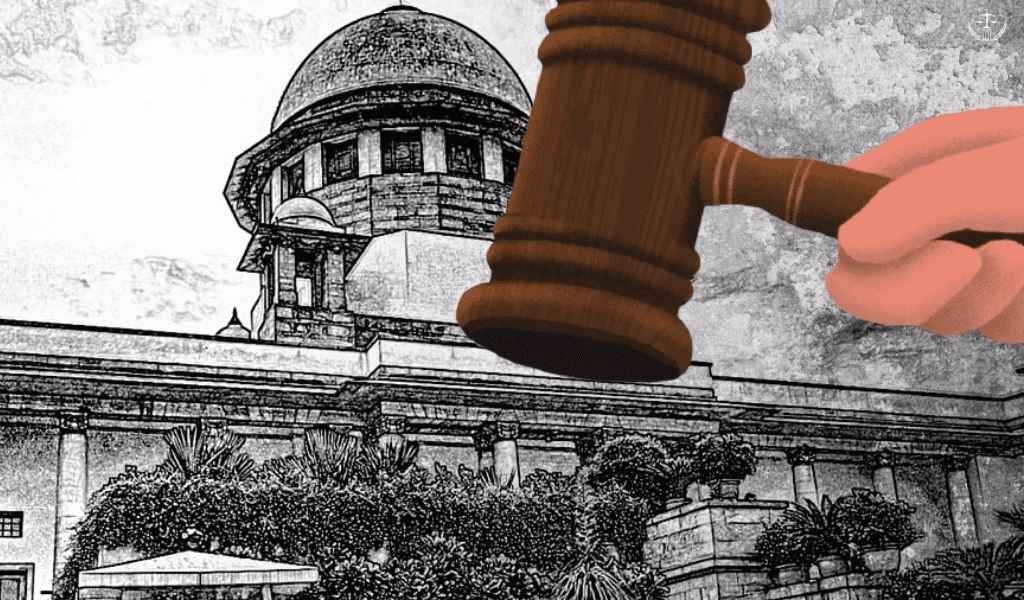
यह भारतीय संविधानिक व्यवस्था में पहली बार हुआ है कि राज्यपाल के दस्तखत के बगैर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई विधेयक कानून बना और तमिलनाडु के सभी 10 लंबित विधेयकों को मंजूरी मिल गई।
बेंच ने कहा कि राज्यपाल के पास पूर्ण या आंशिक वीटो का अधिकार नहीं है। वह विधानसभा से पास बिल को नहीं लटका सकता है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी बताया है कि अगर राज्य का बिल उनके पास आता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट से मशविरा करना होगा और वे भी बिल को तीन महीने से ज्यादा नहीं रोक सकती हैं।
इस तरह से न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को एक आदेश जारी किया और एक परिदृश्य देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे यही लग रहा है कि वे स्वयं ही संविधान की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं।
कहना होगा कि इस समय जिस तरह का बर्ताव हमारे न्यायालय कर रहे हैं, उससे तो भारत की जनता में यही संदेश जा रहा है कि जब सभी निर्णय इन्हें (न्यायपालिका को) लेना है, तब फिर अन्य संविधानिक संस्थाओं की आवश्यकता ही क्या है?
बेकार में संसद, चुनी हुई सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, महापौर, नगर परिषद अध्यक्ष, पंचायती राज में पंच-सरपंच और इस तरह की कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए?
न्यायपालिका एक आदेश और पास कर दे और सब कुछ अपने हाथ में ले ले, कोर्ट ही देश चलाए, बेकार में इतने लोगों पर धन का व्यय हो रहा है!
देश का पैसा भी बचेगा और रोज-रोज का अधिकार एवं कर्तव्यों का जो झगड़ा है, वह भी समाप्त हो जाएगा।
लेख
डॉ. मयंक चतुर्वेदी

